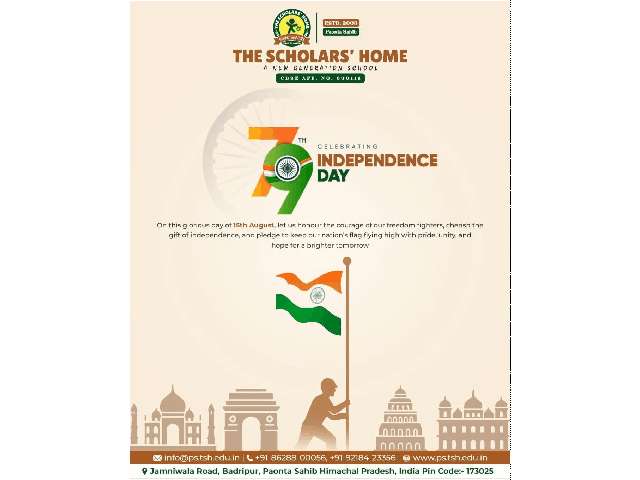
Ashoka Times…6 September 2025
“हिमालयी आपदाएं: चुनौतियाँ और समाधान” पश्चिम हिमालय, जो अपनी सुरम्य वादियों, सदाबहार हिमालयी श्रृंखलाओं और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा और ग्लेशियर पिघलने की घटनाओं में तीव्रता देखी जा रही है। इन घटनाओं के लिए कई बार पर्यावरणीय क्षति, मानवीय लापरवाही या विकास परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन क्या यह सब दोषारोपण उचित है? क्या हमें इस संकट की तह तक जाकर मौसम और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भी समझने की आवश्यकता नहीं? हिमालय और मौसमी अस्थिरता हिमालय, दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला, लगातार भूवैज्ञानिक और मौसमीय बदलावों के अधीन है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्षेत्रीय तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे हिमनदों का पिघलना तेज हो गया है। इसके साथ ही, मॉनसून के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, जिससे वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति अप्रत्याशित हो रही है। ये सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हिमाचल प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रही हैं और आपदाओं की संभावना को बढ़ा रही हैं। विकास और पर्यावरणीय संतुलन विकास की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास सतत नहीं हो सकता। पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध सड़क निर्माण, कटान और जंगलों की कटाई ने मिट्टी के कटाव और भूस्खलन जैसी समस्याओं को बढ़ावा दिया है। लेकिन साथ ही, मौसमी बदलाव और प्राकृतिक चक्रों का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः दोषारोपण के बजाय हमें दोनों पहलुओं को समझ कर संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। समाधान की ओर कदम स्थानीय समुदायों की भागीदारी: पहाड़ी इलाकों में स्थानीय लोगों की पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के बेहतर उपाय किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी: हिमालय की ग्लेशियर गतिविधियों, वर्षा पैटर्न और भू-वैज्ञानिक परिवर्तनों पर लगातार अध्ययन और डेटा संग्रह आवश्यक है। विकास तो सभी चाहते हैं, विनाश नहीं। किसी भी निर्माण से पहले, पर्यावरण का पूरा आकलन होना चाहिए—मलबा कहाँ डालना है, कितने बाँध बनाने हैं, कितने चार-लेन राजमार्ग बनाने हैं। यह सब सोच-समझकर योजनाबद्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मानो अंधी दौड़ चल रही है।क्या किया जाना चाहिए? वास्तव में, सभी नदियों, नालों, नालों और तालाबों का पूरा जोखिम आकलन किया जाना चाहिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्र इसमें मदद कर सकते हैं। निर्माण कार्य ऐसे आकलनों पर आधारित होना चाहिए और नदी या नाले की ज़मीन पर निर्माण प्रतिबंधित होना चाहिए। यह जोखिम आकलन जानकारी पटवारी (स्थानीय राजस्व अधिकारी) स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह सोचना बचकाना है कि हम दीवार बनाकर नदी को रोक सकते हैं। भारी बारिश के दिन, नदी दीवार की ओर नहीं देखती। पहाड़ी नदियाँ अपने साथ पत्थर और शिलाखंड बहाकर ले जाती हैं। धराली नदी को ही देख लीजिए—यह विशाल शिलाखंडों को ढोती हुई खड़ी ढलानों से नीचे उतरती है; कोई भी दीवार इसका सामना कैसे कर सकती है? जलवायु परिवर्तन एक ढाल बन गया है. जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, वर्षा अनियमित हो रही है—कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा—और इससे अचानक बाढ़ आ रही है। पहाड़ों में बाढ़ सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि अचानक बाढ़ होती है। यह पहाड़ों की एक प्राकृतिक विशेषता है। बाढ़ ज़रूरी भी है, क्योंकि यह नदी को साफ़ करती है और मिट्टी और तलछट को बहा ले जाती है जो मैदानों को उपजाऊ बनाती है। लेकिन हकीकत में, जलवायु परिवर्तन सरकारों के लिए एक ढाल बन गया है। यह असली कारणों से ध्यान भटकाता है। सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि असली वजह यह है कि भूमि उपयोग और भूमि आवरण में भारी बदलाव आया है। 2030 तक हमें 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है, लेकिन सतत विकास कैसे होगा? तभी जब योजना सही हो, जब भूमि उपयोग का उचित प्रबंधन हो। ज़रूरत मौसम को कोसने की नहीं, बल्कि उसके प्रति सचेत रहने की है। मौसम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपने काम की योजना बनाएँ। नदी-नालों वाली ज़मीन से दूर रहें—तभी बारिश तबाही में नहीं बदलेगी। साथ ही, यह भी याद रखना होगा कि जब तक व्यवस्था में सुशासन का अभाव रहेगा, पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती और सतत विकास संभव नहीं होगा। सतत विकास की नीति: विकास कार्यों में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन और प्रकृति के अनुकूल तकनीकों का उपयोग जरूरी है। आपदा प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण: आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। निष्कर्ष हिमाचल प्रदेश की सुंदरता और जीवन शैली उसके प्राकृतिक परिवेश पर निर्भर है। मौजूदा संकट के लिए सिर्फ एक कारक को दोष देना उचित नहीं होगा। हमें प्रकृति के संकेतों को समझते हुए, मौसम और पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। तभी हम हिमालय की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।



